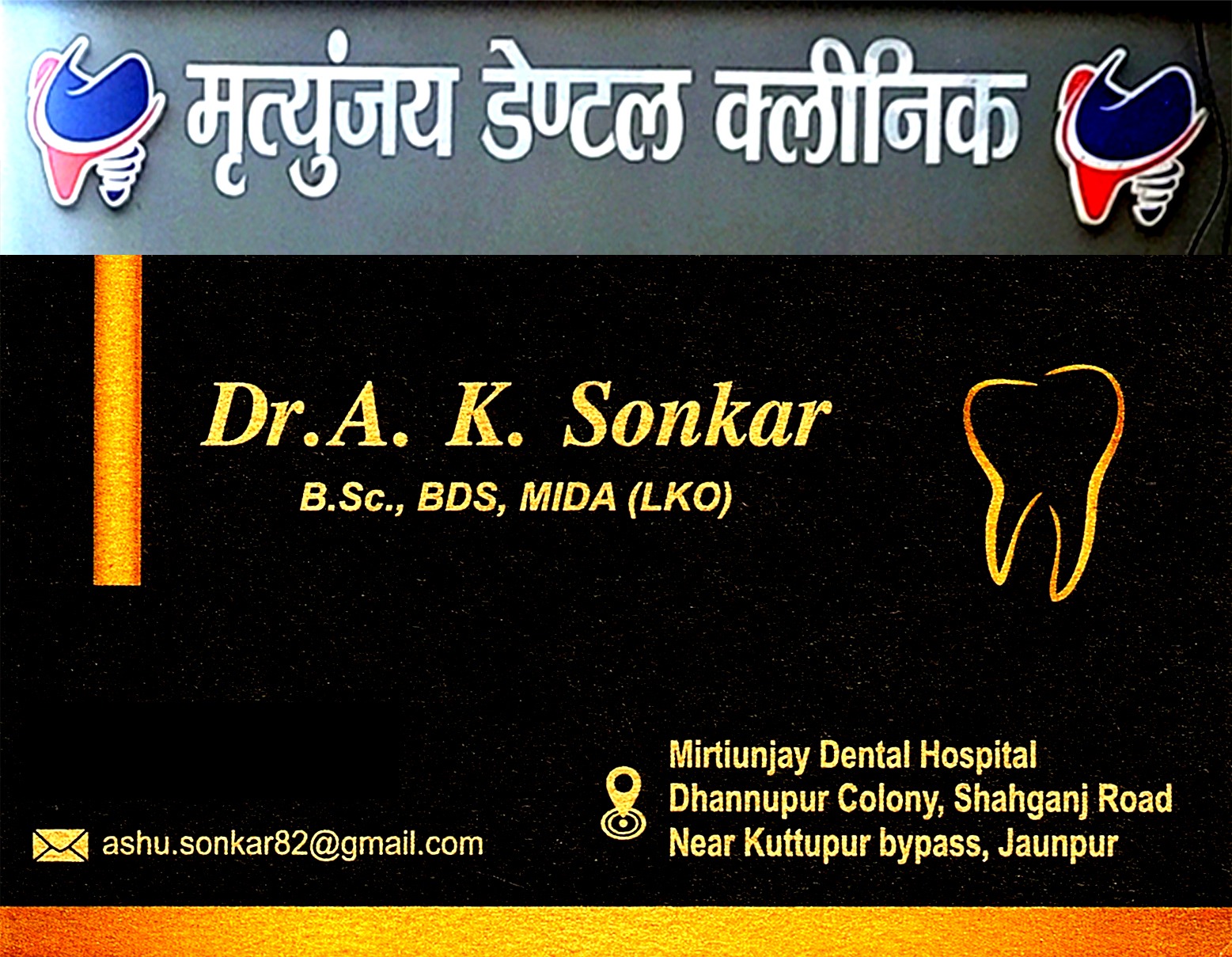पंकज सीबी मिश्रा/पूर्वांचल लाईफ
दशको पहले गांव गिराव की महिलाएं और युवतियां सावन माह का बेसब्री से इंतजार करती थीं। सावन शुरू होते ही दरवाजे से बाहर नीम के पेड़ पर पटेंग वाला झूला पड़ जाता था। ससुराल से बेटियां अपने मायके झूला झूलने आती थी और गाँवो में त्योहारों का गजब रोचक आनंद होता था। पर अब कहा खो गए त्योहार..! कहा गई वो लोकगीत की धुनें..! क्यों नहीं दिखाई देते झूले..! क्यों नहीं सुनाई पड़ती कजरी..! यह सब हमारी अपनी बेवकूफीयों और राजनीतिक लालसा की देन है। सरकारों नें त्योहारों का वजूद खत्म किया और हमने पेड़ काट दिया। आधुनिकता की आंधी में बहुत दूर बह गए और अब छूटे है तो बस ऐसे ही अनमने सवाल जिनके जवाब मै पंकज सीबी मिश्रा अपने इस लेख के माध्यम से आप सबसे पूछ रहा.! बताइयेगा वह हाथों में मेहंदी रचाकर कलाई में हरी चूड़ियां और हरी साड़ी पहनकर बगीचे की ओर निकल पड़नें वाली बेटियां कहा गई.! जो बगीचों की टहनियों पर झूले डालकर दिनभर झूलती रहती थीं। कजरी और सावन गीत गाते हुए आपस में हंसी-ठीठोली करती थीं। छोटे बच्चों के लिए घरों के आंगन में झूला डाला जाता था। सावन के शुरू होते ही मोर, पपीहे और कोयल की मीठी बोली सुनाई देती थी। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में एक चटक रंग है कजरी। मिर्जापुर, बनारस और प्रयागराज के आसपास इलाकों में इसकी मादकता महसूस की जाती थी। हालॉकि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार तक के कई इलाकों में भी पूरी ठसक के साथ विराजती रही। सावन का महीना हो, रिमझिम फुहारे पड़ रही हों, पिया दूर हो, भाई विदा कराने नहीं आया, ननदें छेड़ रही हों, बाबुल का घर याद आ रहा हो, बचपन की सखियां रोज सपने में उलाहना दे रही हों और पेड़ों पर झूले पड़ गए हों तो गोरी के मुंह से जो गीत फूटता है, वही कजरी है। ननद के साथ छेड़छाड़ हो, पति से कोई मांग या उलाहना, कजरी की मस्ती में सभी शामिल है। यानी कजरी में श्रृंगार है, विरह है, छेड़छाड़ है, मान मनुहार है। वह जीवन राग है, जो सावन की फुहारों से भीगे युवा दिलों में धड़कता है। कजरी लोकगायन की सशक्त परंपरा है। यही कारण है कि इसको देश के तमाम बड़े गायकों ने शास्त्रीय और उप शास्त्रीय शैली में भी गाया है। बारिश के इस मौसम में जब तन और मन दोनों से काले बादल गरज कर गोरी को डरा रहे हैं। इन सबके बीच अचानक एक दशक पीछे शिक्षा का स्तर और आधुनिकता बढ़ाने के नाम पर हमने इन सभी परम्पराओ का विनाश कर लिया। किसी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर इससे भी पता नहीं चलता कि उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं। किसी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर इससे पता चलता है कि उसने खुद की कितनी स्वतंत्र सोच विकसित की है। तथ्यों, प्रमाणों का कितना तार्किक विश्लेषण वह कर पाता है। व्यक्ति चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, अगर वह अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाया तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कि वो कितना पढ़ा है। आधुनिकता के दौर में विशालकाय पेड़, बगीचे, मोर, पपीहे, और कोयल की गूंज भी गायब हो गए। अब अधिकतर घरों के युवा गांव में नहीं रहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर ही रहने लगे हैं। शहर में ही नौकरी और व्यवसाय कर वहीं बस गए हैं। गांव में अब पुराने लोग ही रह गए हैं। जो हैं भी वह शहरियों की नकल करने लगे हैं। अब शहर व ग्रामीण इलाकों में न तो कहीं झूले दिखाई देते हैं और न ही सावन के गीत सुनाई देते हैं। गांव में 60 फुट से गहरे कुएं होते थे। इनमें पीने का पानी भरने के लिए गांव के हर परिवार में रस्सी भी होती थी। वही रस्सी सावन में झूला डालने के काम आती थी। अब कुएं खत्म हो गए तो रस्सी देखने को भी नहीं मिलती है। झूले बस याद बनकर रह गए हैं।आपकी शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि आप सवाल करें कि हवन में देसी घी जलाने पर कैसे आक्सीजन का निर्माण होता है। कैसे गाय पर हाथ फेरने से ही कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। कैसे गाय का गोबर परमाणु विकिरण से बचा सकता है। सनातन धर्मो की पौराणिक कहानियां दरअसल हमारे लिए हमारी संस्कृति और त्योहारों को बचाने का साधन हुआ करती थी। एक प्रश्न पत्र हमारे ज्ञान की, तर्क शक्ति की परीक्षा लेती हैं। लेकिन अफसोस इस परीक्षा में अधिकतर फेल ही होते हैं। दरअसल हम सब डिग्री धारी जरूर हैं लेकिन ज्ञान धारी नही। डिग्री हमने केवल नौकरी पाने के लिए ली है जीवन जीने के लिए नही ली।
बतकही : गाँवों से विलुप्त हुई कजरी, दिखते नहीं झूले, ना ही सुनाई देते है लोकगीत